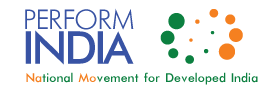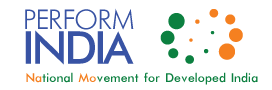प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने नौ साल पूरे कर लिए हैं। इन नौ सालों में पीएम मोदी ने हर उस सेक्टर पर ध्यान दिया है जिससे देश तरक्की की राह पर रफ्तार भर सके। किसी भी देश के विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर का अहम रोल होता है और मोदी सरकार ने पर्वतमाला, भारतमाला, सागरमाला के जरिये जल, थल और पर्वतीय इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर दिया है। पीएम मोदी ने देश को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए पर्वतीय राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को लेकर 2001 में अपना विजन रख दिया था। जबकि उस वक्त वह किसी संवैधानिक पद पर भी नहीं थे बल्कि के एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपनी बातें कही थी। पीएम मोदी के विजन के अनुरूप पर्वतमाला आज भारत के पर्वतीय क्षेत्रों की सुरक्षा और विकास को नई ऊर्जा दे रही है। वहीं भारतमाला और सागरमाला प्रोजेक्ट के जरिये भारत में विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्गों, सामरिक सड़कों के निर्माण, बंदरगाह और तटीय क्षेत्र की सुरक्षा को गति देने के साथ ही देश के पर्वतीय क्षेत्रों खासकर सीमांत गांवों के समावेशी विकास के लिए पर्वतमाला प्रोजेक्ट के जरिये एक मजबूत ब्लू प्रिंट तैयार कर इस पर काम किया जा रहा है।
 पीएम मोदी ने 2001 में दिया था पर्वतमाला का विजन
पीएम मोदी ने 2001 में दिया था पर्वतमाला का विजन पर्वतीय राज्य उत्तराखंड के दौरे पर 21 अक्टूबर 2022 को केदारनाथ पहुंचे पीएम मोदी ने 3400 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। लेकिन पर्वतीय राज्यों के लिए अपने विजन उन्होंने 2001 में स्पष्ट कर दिए थे। उस वक्त वह किसी संवैधानिक पद पर भी नहीं थे बल्कि के एक कार्यकर्ता के रूप में अपनी बातें कही थी। उन्होंने कहा था- ”इंफॉरमेशन टेक्नोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, चहुं दिशा में जनता में ये विश्वास पैदा होना चाहिए। कुछ क्षेत्रों में तो तबाही की गर्त में डूब गया। उत्तरांचल हमने बनाया, हम कहते थे कि छोटे राज्य बेकार है। उद्योगों को अवसर नहीं मिला है, हमें इस परिस्थिति को पलटना है। हमें उत्तरांचली का जो मिजाज है उसे बनाए रखना है, बचाए रखना है। उत्तरांचली की पहचान बनाना है मुझे। हम यहां टूरिज्म को दो हिस्सों में विकसित करना चाहते हैं। एक है स्पिरिचुअल टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म को बरकरार रखना है। उसके साथ साथ आज की पीढ़ी कुछ और आवश्यताएं चाहती हैं। उत्तरांचल के पास 100 करोड़ का बाजार पड़ा है। हंड्रेड करोड़ का बाजार है। इस देश में पैदा होने वाला हर नागरिक गंगा में गोता लगाने के लिए आना चाहता है। इस देश में पैदा हुआ हर नागरिक मौका मिले तो अपने मां-बाप केदारनाथ, बद्रीनाथ ले जाना चाहता है। 100 करोड़ का मार्केट है आपके साथ। ये आपकी योजना चाहिए कि 100 करोड़ देशवासी आसानी से यहां आएं और उनका स्वागत हो।”
#ModiInDevBhumi As PM @narendramodi today addressed the nation from Mana, Uttarakhand, we present an archival video from 2001 (even before he became Gujarat’s Chief Minister) showcasing the same vision he is bringing to life today!
1/2 pic.twitter.com/B1CxlKac3f
— Modi Archive (@modiarchive) October 21, 2022
पर्वतमाला परियोजना से पर्वतीय क्षेत्रों की सुरक्षा और विकास को मिलेगी धार
भारत के पर्वतीय क्षेत्रों की सुरक्षा रणनीति में अहमियत को चीन के सैन्य विशेषज्ञों के वक्तव्य के जरिये जाना जा सकता है। वर्ष 2020 में जब कोरोना महामारी की शुरुआत हो चुकी थी, ऐसे समय में चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के लिए सैन्य साजो-सामान बनाने से जुड़े एक मिलिट्री एक्सपर्ट ने कहा था कि ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भारत के पास विश्व के सबसे ज्यादा अनुभवी सैनिक हैं और पर्वतीय इलाकों में तैनाती के लिए हर भारतीय सैनिक के पास पर्वतारोहण का अनिवार्य स्किल है। वहीं ‘माडर्न वीपनरी मैग्जिन के सीनियर एडिटर हुआंग गुओझी ने भी कहा था, ‘वर्तमान में मैदानी और पर्वतीय इलाकों में दुनिया की सबसे ज्यादा अनुभवी सेना अमेरिका, रूस या यूरोपीय महाशक्ति के पास नहीं, बल्कि यह भारत के पास है।
पर्वतमाला का उद्देश्य : विकास के साथ पर्यटन को मिलेगी गति
पर्यटन भारत जैसे विकासशील देश के जीडीपी ग्रोथ का एक महत्वपूर्ण आधार है और इसी बात को ध्यान में रखकर 2022-23 के बजट के तहत केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के बजट में 18.42 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है और इसके लिए 2400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पर्यटन क्षेत्र को गति देने की ही खास योजना पर्वतमाला है। पर्यटन को रफ्तार देने के लिए यह योजना लाभकारी सिद्ध होगी। खास बात यह है कि महिला पर्यटकों की सुरक्षा पर भी 5.27 करोड़ रुपये का प्रवधान किया गया है। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने में मदद मिलेगी। इसी उद्देश्य से पहाड़ी राज्यों को केंद्रीय बजट 2022-23 में आठ रोपवे की सौगात मिली है। इन राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर के कुछ राज्य शामिल हैं। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत पर्वतमाला को पीपीपी मोड से चलाया जाएगा। 2022-23 में इन पहाड़ी राज्यों में 60 किमी लंबे आठ रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। पर्वतीय राज्यों में सड़क निर्माण काफी कठिन होता है। ऐसे में रोपवे से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इससे रोजगार के मौके भी उपलब्ध होंगे। इन रोपवे परियोजनाओं को आधुनिक तकनीक से तैयार किया जाएगा, ताकि सुरक्षा भी बनी रहे।
 पर्वतमाला चीन से लगती सीमा की सुरक्षा में भी अहम
पर्वतमाला चीन से लगती सीमा की सुरक्षा में भी अहमभारत चीन के साथ 3,488 किमी लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। जिन भारतीय राज्यों की सीमा चीन से लगती है वे सभी पर्वतीय राज्य हैं। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर चीन से 1597 किमी, हिमाचल प्रदेश से 200 किमी, उत्तराखंड से 345 किमी, सिक्किम से 220 किमी और अरुणाचल प्रदेश से 1126 किमी लंबी सीमा साझा होती है। भारत के इन पर्वतीय राज्यों में चीन के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने के चलते कई तरीके की सुरक्षा और उससे जुड़ी कई अन्य चुनौतियां हैं। इन पांच पर्वतीय राज्यों के सीमा पर स्थित गांवों में अक्सर चीन द्वारा अतिक्रमण की घटनाएं सामने आई हैं। दरअसल आजादी से 60 वर्षों तक सीमांत गांवों अथवा भारत के अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित संवेदनशील क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की मुख्यधारा में नहीं आ पाए थे।
देश की सुरक्षा अवसंरचना पर हो रहा है तेजी से काम
चाहे भारत द्वारा श्योक नदी से दौलत बेग ओल्डी तक 235 किमी लंबे अति सामरिक महत्व के सड़क का निर्माण हो, सिक्किम में भारत चीन सीमा से मात्र 60 किमी दूर स्थित सामरिक महत्व वाले पाकयोंग हवाई अड्डे का उद्घाटन हो, भारतीय वायु सेना द्वारा यहां पर अपने सबसे विशालकाय विमान एएन-32 उतारने की घटना हो, पर्वतीय क्षेत्रों में नौसेना के टोही विमान डोर्नियर की भी उपस्थिति हो, चीन को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर संतुलित करने हेतु भारतीय सेना द्वारा डोकलाम प्रकरण के बाद बार्डर रोड आर्गेनाईजेशन के साथ मिलकर तीन नई सड़कों के निर्माण का कार्य हो, तवांग और बूमला सेक्टर्स के पास सेला दर्रे के पास भारत एक महत्वाकांक्षी सुरंग निर्माण को भी अंजाम दे रहा है। सेला दर्रे के पास 317 किमी लंबे बालीपाड़ा-चारद्वार-तवांग एक्सिस पर भारत दो सैन्य महत्व की दो सुरंगे भी बना रहा है। इसमें से एक टू लेन टनल 13 हजार फीट से भी अधिक ऊंचाई पर और दूसरा सबसे लंबा टनल है। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में भारत ने अपने सुरक्षा अवसंरचना के विकास को तेजी दी है।
लद्दाख में 19,300 फीट से अधिक की ऊंचाई पर सड़क का निर्माण एक नया कीर्तिमान
सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रे के पास 19,300 फीट से अधिक की ऊंचाई पर मोटर वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण कर विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उमलिंगला दर्रे से होकर गुजरने वाली 52 किमी लंबी यह सड़क तारकोल से बनाई गई है। उमलिंगला पास अब एक ब्लैक टाप सड़क से जुड़ गया है। पूर्वी लद्दाख में इस सड़क के निर्माण से क्षेत्र के चुमार सेक्टर के सभी महत्वपूर्ण कस्बे आपस में जुड़ जाएंगे। चिशुमले और देमचोक के लेह से सीधे आवागमन का वैकल्पिक मार्ग का विकल्प उपलब्ध कराने के कारण इस सड़क का स्थानीय लोगों के लिए काफी महत्व है। इसकी मदद से सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और लद्दाख में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
 पलायन रोकने और सीमांत गांव को फिर से बसाने की मुहिम
पलायन रोकने और सीमांत गांव को फिर से बसाने की मुहिमउत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की सुरक्षा हाल के समय में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की सुरक्षा पलायन करने वाले सीमांत गांव को फिर से बसाने, इस क्षेत्र में पर्यटन को मजबूत धार देकर रोजगार सृजन करने के प्रयास तेज हुए हैं। प्रदेश के पर्वतीय जिलों में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों पर विशेष तौर से फोकस करने की रणनीति बनाई गई है। पर्वतीय क्षेत्रों के विकास से जुड़ी रणनीति में सीमांत गांवों से पलायन को रोकने और पलायन से खाली हो चुके गांवों में ग्रामीणों को पुन: बसाने पर स्लोवेनिया की तरह जोर दिया गया है। गौरतलब है कि स्लोवेनिया अपने कुल राजस्व का 30 प्रतिशत पर्यटन से ही प्राप्त करता है।
उत्तरकाशी में गरतांग गली का जीर्णोद्धार
सरकार ने उत्तरकाशी स्थित गरतांग गली का जीर्णोद्धार कर उसे उत्तराखंड के पर्यटन की मुख्य धारा से जोड़ दिया है। यह लकड़ी का पुल भारत और तिब्बत के बीच का व्यापार मार्ग था। नामधारी (भोटिया जनजाति) समुदाय जो इस व्यापार का मुख्य संवाहक था, उसके प्रयासों को प्रतिष्ठित किया गया है। वहीं चीन से लगे उत्तराखंड के नेलांग घाटी के विकास के लिए ऐसी नीति बनाई गई है जिससे इनर लाइन परमिट जैसे प्रावधान पर्यटन और विकास के मार्ग में बाधा न बन सकें।
पर्वतमाला प्रोजेक्ट से उत्तराखंड में 27 प्रोजेक्ट पर काम
पर्वतमाला प्रोजेक्ट से रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ, चमोली जिले में गोविंदघाट- घांघरिया समेत उत्तराखंड में 27 प्रोजेक्टों के धरातल पर उतरने की आस भी बढ़ी है। इससे पहाड़ी राज्यों में परिवहन के आधुनिक साधनों की व्यवस्था की जाएगी। इसमें बार्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर विशेष फोकस किया गया है। देश की उत्तरी सीमा से लगते गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज योजना से उत्तराखंड के पांच जिलों में सीमांत पर स्थित 1107 गांवों को इसका लाभ मिल सकता है।
सागरमाला परियोजनाः 567 परियोजनाओं पर अनुमानित लागत 58,700 करोड़ रुपये
मोदी सरकार की सागरमाला कार्यक्रम की सफलता के आधार पर, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने “तटीय जिलों के समग्र विकास” के लिए सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 567 परियोजनाओं की पहचान की है, जिसकी अनुमानित लागत 58,700 करोड़ रुपये है। सागरमाला बंदरगाह आधारित परियोजना है और आवागमन लागत में कमी और आयात-निर्यात प्रतिस्पर्धा पर ध्यान केंद्रित करती है। इसके अंतर्गत तटीय जिलों के समग्र विकास का उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में मौजूद अंतराल को पाटना और आर्थिक अवसर में सुधार करना है। तटीय जिलों के समग्र विकास में पहचानी गई परियोजनाओं और सागरमाला परियोजना के अंतर्गत प्राप्त नई योजनाओं के प्रस्तावों के साथ, कुल परियोजनाओं की संख्या 1537 है और इन पर कुल 6.5 लाख करोड़ रुपये की लागत आएगी।
 सागरमाला के तहत 45,000 करोड़ रुपये लागत से 29 परियोजनाएं पूरी
सागरमाला के तहत 45,000 करोड़ रुपये लागत से 29 परियोजनाएं पूरीसागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत 5.5 लाख करोड़ रुपये लागत की 802 परियोजनाएं हैं, जिन्हें वर्ष 2035 तक कार्यान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 99,281 करोड़ रुपये लागत की 202 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। सार्वजनिक-निजी भागीदारी-पीपीपी मॉडल के अंतर्गत 45,000 करोड़ रुपये लागत से कुल 29 परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी जा चुकी हैं, जिससे सरकारी खजाने पर वित्तीय बोझ कम हुआ है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत अतिरिक्त 32 परियोजनाएं 51,000 करोड़ रुपये की लागत से वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही हैं। इसके अलावा, 2.12 लाख करोड़ रुपये की 200 से अधिक परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और इनके 2 वर्ष में पूरा होने की आशा है।
फ्लोटिंग जेट्टी के विकास के लिए 200 स्थानों की पहचान
मंत्रालय अब तक 140 परियोजनाओं के लिए 8748 करोड़ रुपये का अनुदान दे चुका है और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए अतिरिक्त प्रस्तावों की समीक्षा कर रहा है। फ्लोटिंग जेट्टी यानी तैरते हुए घाट के विकास के लिए 200 से अधिक स्थानों की पहचान की गई है और 50 स्थानों को चरण 1 के कार्यान्वयन का हिस्सा बनाया गया है। इसके साथ ही 33 मत्स्य बंदरगाह परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें से 22 मत्स्य बंदरगाह परियोजनाओं के लिए 2400 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। राष्ट्रीय सागरमाला कार्यक्रम से देश के समुद्री व्यापार के व्यापक विकास और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। कार्यक्रम के अंतर्गत, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने इस परियोजना के आरंभ होने के बाद से बड़े पैमाने पर विभिन्न परियोजनाओं को लागू किया है। इन परियोजनाओं में बंदरगाह आधुनिकीकरण, सम्पर्क, औद्योगीकरण, सामुदायिक विकास, तटीय पोत परिवहन और अंतर्देशीय जलमार्ग विकास शामिल हैं। इस तरह के प्रयास के परिणामस्वरूप, राष्ट्र ने बढ़ी हुई क्षमता, दक्षता, रोजगार सृजन, निजी भागीदारी में वृद्धि, आने-जाने के समय में कमी, परिवहन लागत में कमी, व्यापार करने में सुगमता में वृद्धि और भारत को प्रमुख समुद्री राष्ट्रों के वैश्विक मानचित्र में शामिल करने जैसी विभिन्न उपलब्धियां हासिल की हैं।
बंदरगाहों की स्थापित क्षमता 1531 से बढ़कर 2554.61 एमटीपीए हो गई
सरकार ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लागत और आवागमन के समय को कम करने के लिए बंदरगाहों पर कई आधुनिकीकरण, मशीनीकरण और डिजिटल परिवर्तन के उपाय किए हैं जैसे डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी, डायरेक्ट पोर्ट एंट्री, कंटेनर स्कैनर और आरएफआईडी (रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन) सिस्टम की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा, शिपिंग ईकोसिस्टम के लिए शुरू से अंत तक व्यापार सुविधा प्रदान करने के लिए पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम (पीसीएस 1 एक्स) को एनपीएल-एमएआरआईएनई में अपग्रेड किया जा रहा है। चूंकि बंदरगाह देश के आयात-निर्यात व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सरकार का ध्यान बंदरगाहों की क्षमता वृद्धि पर बना रहता है ताकि वे देश की बढ़ती वाणिज्यिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हों। वर्ष 2014-15 के दौरान भारतीय बंदरगाहों की स्थापित क्षमता 1531 एमटीपीए थी, जो अब वर्ष 2020-21 में बढ़कर 2554.61 एमटीपीए हो गई है।
 बंदरगाहों पर यातायात में 6.94 प्रतिशत की वृद्धि
बंदरगाहों पर यातायात में 6.94 प्रतिशत की वृद्धिवित्त वर्ष 2021-22 के दौरान प्रमुख बंदरगाहों पर हुए यातायात में पिछले वर्ष की तुलना में 6.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। पांच प्रमुख बंदरगाहों ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान अपना अब तक का सबसे अधिक यातायात दर्ज किया। कामराज बंदरगाह पर पिछले वर्ष की तुलना में 49.63 प्रतिशत यातायात की वृद्धि दर्ज की गई। जेएनपीटी ने पिछले वर्ष की तुलना में 17.27 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि के साथ इसी अवधि के दौरान अब तक का सबसे अधिक यातायात हासिल किया। दीनदयाल बंदरगाह ने भी 8.11 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर की और 127.1 मिलियन टन के अपने उच्चतम लदान को भी प्राप्त किया। मुंबई बंदरगाह ने पिछले वर्ष की तुलना में 11.46 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। कोचीन बंदरगाह ने वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर 9.68 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की और अपने अब तक के उच्चतम यातायात को भी प्राप्त किया। यह विभिन्न बंदरगाहों पर नए बर्थ और टर्मिनलों के निर्माण, मौजूदा बर्थ और टर्मिनलों के मशीनीकरण, पोर्ट चैनलों में बड़े जहाजों को आकर्षित करने के लिए ड्राफ्ट को गहरा करने के लिए कैपिटल ड्रेजिंग के लिए शुरू की गई विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कारण संभव हुआ है। कुल औसत टर्न अराउंड समय वर्ष 2014-15 में 96 घंटे से घटकर 2021-22 में 52.80 घंटे हो गया, जबकि प्रमुख बंदरगाहों पर कंटेनर औसत टर्न अराउंड समय भी वर्ष 2014-15 में 35.21 घंटे से घटकर 2021-22 में 27.22 घंटे हो गया है।
मुंबई और मोरमुगाओ बंदरगाह में दो विशाल क्रूज टर्मिनल बनाई जा रही
मुंबई और मोरमुगाओ बंदरगाह में सागरमाला परियोजना के माध्यम से दो विशाल क्रूज टर्मिनल परियोजनाएं भी विकसित किया जा रहा है। मुंबई में अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उन्नयन और आधुनिकीकरण 303 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन है। इस परियोजना का 70 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा हो गया है। मंत्रालय मोरमुगाओ बंदरगाह पर अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रूज टर्मिनल तथा संबद्ध सुविधाओं के विकास के लिए भी सहायता कर रहा है। मंत्रालय जलमार्ग के माध्यम से रो-रो और यात्री परिवहन को बड़ा बढ़ावा दे रहा है क्योंकि यह आवागमन के लिए पर्यावरण के अनुकूल सुविधा है और इसके परिणामस्वरूप लागत तथा समय की महत्वपूर्ण बचत होती है। रोपैक्स सुविधाएं राज्य या केंद्रीय प्राधिकरणों द्वारा विकसित की जा रही हैं और जहाजों की तैनाती तथा सेवाएं प्रमुख रूप से निजी कम्पनियों द्वारा प्रदान की जाती हैं। शहरी जल परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक फेरी के उपयोग को बढ़ावा देते हुए दीर्घकालिक अनुबंध पर ओ एंड एम के लिए नए व्यापार मॉडल विकसित करने की भी योजना है। प्रचालन चरण के दौरान उपयुक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हितधारकों के परामर्श से अलग योजना तैयार की जाएगी।
वर्ष 2025 तक 340 मीट्रिक टन तक तटीय शिपिंग की अतिरिक्त क्षमता होगी
सागरमाला के अंतर्गत किए गए अध्ययनों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 तक लगभग 340 मीट्रिक टन तक तटीय शिपिंग की एक अतिरिक्त क्षमता है, जिसकी अनुमानित वार्षिक लागत 9600 करोड़ रुपये की बचत होगी। कोयला, इस्पात, सीमेंट, ऑटोमोबाइल, खाद्यान्न, उर्वरक, पीओएल, आदि तटीय पोत परिवहन के माध्यम से लाने-ले जाने वाली प्रमुख वस्तुएं हैं। तटीय पोत परिवहन को बढ़ावा देने के एक हिस्से के रूप में, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत “सागरमाला तटीय पोत परिवहन निगरानी समिति” बनाने का प्रस्ताव है, जो सागरमाला योजना की प्रगति की निगरानी करेगी और बुनियादी ढांचे को वित्त पोषण सहायता प्रदान करेगी। जहाज़ों की आवाजाही की सुविधा और जमीनी स्तर पर बुनियादी ढांचे को सक्षम करने के लिए, समर्पित सागरमाला तटीय पोत परिवहन नोडल अधिकारी ने प्रत्येक प्रमुख और गैर-प्रमुख बंदरगाहों पर योजना बनाई। अंतर्देशीय जलमार्ग अंतरशहरी आवागमन, कम दूरी के यात्री परिवहन की जरूरतों के लिए एक व्यवहार्य माध्यम बन सकते हैं। फेरी, रो-पैक्स जहाजों और हाई-स्पीड लॉन्च के माध्यम से, राज्य सरकारें और शहरी स्थानीय निकाय शहरी और उपनगरीय आबादी को निर्बाध, एकीकृत परिवहन सेवाएं प्रदान कर सकते हैं और दैनिक आवागमन के तनाव और भीड़ को कम कर सकते हैं।
 मल्टी-मॉडल हरित और सस्ते परिवहन के मॉडल पर जोर
मल्टी-मॉडल हरित और सस्ते परिवहन के मॉडल पर जोर कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 23 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक नौकाओं की खरीद की है। ऐसे प्रत्येक जहाज में 100 यात्रियों को ले जाने की क्षमता है। आईडब्ल्यूएआई ने 5 स्थानों : वाराणसी, कोलकाता, पटना और गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ के लिए समान सेवाओं का प्रस्ताव दिया है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस मॉडल की सिफारिश की है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे मल्टी-मॉडल हरित और सस्ते परिवहन के मॉडल को अपनाएं।
जलमार्ग से 200 टन खाद्यान्न और 2000 टन स्टील भेजे गए
पर्यावरण के अनुकूल और किफायती तरीके से थोक वस्तुओं की आवाजाही को सक्षम करने के लिए अंतर्देशीय जल परिवहन भी एक प्रभावी तरीका हो सकता है। आईडब्ल्यूएआई ने इस वर्ष की शुरुआत में, भारत और बांग्लादेश में गंगा, हुगली, मेघना तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के माध्यम से पटना और गुवाहाटी के बीच 200 टन खाद्यान्न और हल्दिया तथा गुवाहाटी के बीच 2000 टन स्टील पहुंचाने का सफल यात्रा का संचालन किया है। अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में इस अभियान की क्षमता को उजागर करता है। इस मॉडल को कोयला, एलपीजी, उर्वरक कंटेनरों सहित अन्य थोक वस्तुओं के परिवहन के लिए दोहराया और बढ़ाया जा सकता है तथा इसे तटीय शिपिंग के साथ एकीकृत किया जा सकता है। पूर्वोत्तर राज्य कम दूरी और भीड़-भाड़ मुक्त परिवहन के लिए लाभान्वित हो सकते हैं।
 भारतमाला के तहत दिल्ली-मुबंई सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे
भारतमाला के तहत दिल्ली-मुबंई सबसे बड़ा एक्सप्रेसवेभारतमाला परियोजना के तहत 1,386 किलोमीटर के देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का विकास किया जा रहा है, जिसका दिल्ली-दौसा-लालसोट सेक्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को समर्पित कर चुके हैं।
देश में 9 साल में लगभग 50,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने
देश में पिछले नौ साल में लगभग 50,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ है। देश में 2014-15 में नेशनल हाईवे कुल 97,830 किलोमीटर था, जो मार्च, 2023 तक बढ़कर 1,45,155 किलोमीटर हो गया है। आंकड़ों के अनुसार, 2014-15 में प्रतिदिन 12.1 किलोमीटर सड़क निर्माण से 2021-22 में देश में सड़क निर्माण की रफ्तार बढ़कर 28.6 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है। सड़क और राजमार्ग की किसी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सड़क परिवहन न केवल आर्थिक विकास बल्कि सामाजिक विकास, रक्षा क्षेत्रों के साथ-साथ जीवन की बुनियादी चीजों तक पहुंच का आधार है।
70 फीसदी माल ढुलाई सड़क मार्ग से होती है
एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रति वर्ष लगभग 85 फीसदी यात्री और 70 फीसदी माल ढुलाई सड़क मार्ग से होती है। इससे राजमार्गों के महत्व का पता चलता है। भारत में लगभग 63.73 लाख किमी सड़क नेटवर्क है, जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है।
 भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 2,921 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण
भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 2,921 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माणअगस्त 2020 तक कुल 12,413 किलोमीटर की लंबाई वाली 322 सड़क परियोजनाओं को भारतमाला परियोजना के तहत आवंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त, इसी तारीख तक इस परियोजना के अंतर्गत 2,921 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण किया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की विस्तृत समीक्षा की है और 5,35,000 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय पर लगभग 34,800 किलोमीटर लंबाई की सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में शेष 10,000 किलोमीटर के विस्तार सहित) के विकास के लिए भारतमाला परियोजना के पहले चरण के तहत समग्र निवेश करने की स्वीकृति प्रदान की है। ‘भारतमाला परियोजना’ राजमार्ग क्षेत्रों के लिए सड़क निर्माण का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो मुख्य आर्थिक गलियारों, आंतरिक गलियारों और प्रमुख मार्गों, राष्ट्रीय गलियारों में दक्षता सुधार, सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कें, तटीय और पोर्ट कनेक्टिविटी सड़कें बनाने तथा ग्रीन-फील्ड(हरित) एक्सप्रेसवे के विकास जैसी प्रभावी योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को पूरा करके देश भर में माल और यात्री गतिविधियों की दक्षता को अनुकूलित करने पर केंद्रित है।
भारतमाला के तहत बन रहे 9000 किलोमीटर लंबाई में आर्थिक गलियारे
भारतमाला परियोजना के तहत संपूर्ण भारत के सभी प्रमुख स्थानों को राजमार्गों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें लगभग 9000 किलोमीटर लंबाई में आर्थिक गलियारे अर्थात इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का लक्ष्य है। इसके अलावा इंटर कॉरिडोर और फिडर रोड़ की 6000 किलोमीटर लंबी सड़कों का लक्ष्य भी इस परियोजना के तहत रखा गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के नवीनीकरण के अलावा लगभग 5000 किलोमीटर लंबी नऐ राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का लक्ष्य भी इस परियोजना का एक अहम अंग है। इसके अलावा परियोजना के लक्ष्यों में सीमा क्षेत्रों में राजमार्गों के लिए 2000 किलोमीटर लंबी सड़कों का लक्ष्य रखा गया है। जबकि तटीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण का यह लक्ष्य लगभग 2000 किलोमीटर का रखा गया है। तटीय क्षेत्रों में यह इन राजमार्गों को सागरमाला परियोजना के साथ जोड़ दिया जाएगा।
800 किलोमीटर लंबे ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण का लक्ष्य
सागरमाला परियोजना के तहत लगभग 800 किलोमीटर लंबे ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण का लक्ष्य भी रखा गया है। इस तरह इस परियोजना में विशुद्ध रूप से लगभग 24800 किलोमीटर लंबे नए राजमार्ग एवं एक्सप्रेस वे के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। यह 24800 किलो मीटर का लक्ष्य संपूर्ण भारतमाला परियोजना का लक्ष्य न होकर महज इसके प्रथम चरण का लक्ष्य है। इसके एकीकृत प्रथम चरण का कुल लक्ष्य 34800 किलोमीटर है, जोकि 10000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के बचे हुए लक्ष्य को सम्मिलित कर लेने पर होता है। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम सन 1998 में भारत में वाजपेयी सरकार के समय लाया गया था।
भारतमाला में 10 करोड़ मानवीय श्रम दिवसों का सृजन होगा
भारतमाला परियोजना में सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार 10 करोड मानवीय श्रम दिवसों का सृजन होगा। इनके अलावा लगभग 22000000 नियमित रोजगारों का सृजन भी इस परियोजना के द्वारा होगा। जिससे इस परियोजना की विशालता का अनुमान लगाना संभव हो सकता है। भारतमाला परियोजना के प्रथम चरण की लागत का आकलन लगभग 535000 करोड़ रुपए आंका गया है। इस भारी भरकम रकम की प्राप्ति कई मदों में की जाएगी। भारतमाला परियोजना के दूसरे चरण में तकरीबन 30600 किलोमीटर लंबे सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार भारत माला परियोजना में निर्मित सड़कों की कुल लंबाई 65400 किलोमीटर होगी। इस परियोजना के द्वितीय चरण की लागत के आधिकारिक आकलन अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। परियोजना के प्रथम चरण की शुरुआत 2018 में हुई जबकि परियोजना का प्रथम चरण सन 2022 में संपन्न होगा।
भारतमाला परियोजना के तहत 50 आर्थिक गलियारे होंगे
भारत में वर्तमान में 6 आर्थिक गलियारे अर्थात इकोनॉमिक कॉरिडोर है। संपूर्ण भारत माला परियोजना के तहत 44 नए आर्थिक गलियारे अर्थात इकोनॉमिक कॉरिडोरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इन सबको मिलाकर भारत में भारतमाला परियोजना की सफलतापूर्वक पूरी होने पर 50 आर्थिक गलियारे अथवा इकोनॉमि कॉरिडोर होंगे। भारतमाला परियोजना गुजरात और राजस्थान से आरंभ होकर पंजाब उसके बाद जम्मू कश्मीर तदोपरांत क्रमशः हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए नॉर्थ ईस्ट राज्यों की तरफ जाएगी। जिनमें सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम आदि राज्यों को एक सूत्र में बांधने का काम करेगी।
5300 किलोमीटर सड़कों का निर्माण सीमा क्षेत्रों में
इस परियोजना के अंतर्गत 5300 किलोमीटर लंबे राजमार्ग एवं सड़कों का निर्माण सीमा क्षेत्रों में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मयानमार और बांग्लादेश से लगी सीमाओं पर होगा। परियोजना के द्वितीय चरण में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में होगा। द्वितीय चरण में यह परियोजना सागरमाला परियोजना के साथ मिल जाएगी और तटीय क्षेत्रों में सागरमाला परियोजना के साथ-साथ बंदरगाहों से संपर्कता बेहद सुगम हो पाएगी।
कतर को पीछे छोड़ भारत ने सड़क निर्माण में बनाया विश्व रिकॉर्ड
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश के आधारभूत ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। इसका परिणाम है कि इस क्षेत्र में रोज नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग ने महाराष्ट्र में NH-53 पर अमरावती से अकोला के बीच 105 घंटे और 33 मिनट यानि 5 दिन से भी कम समय में 75 किमी लंबी सड़क बनाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। इससे पहले सबसे तेज सड़क बनाने का रिकॉर्ड कतर के नाम था। कतर के दोहा में फरवरी 2019 में 25.275 किलोमीटर लंबी सड़क तैयार कर रिकॉर्ड बनाया गया था। इसे पूरा करने में 10 दिन का समय लगा था।
राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रतिदिन विस्तार में तीन गुना बढ़ोतरी
केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद से देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में काफी प्रगति हुई है। राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रतिदिन विस्तार में तीन गुना बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों के अनुसार, 2014-15 में प्रतिदिन 12.1 किलोमीटर सड़क निर्माण से 2021-22 में देश में सड़क निर्माण की रफ्तार बढ़कर 28.6 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है। इसी तरह सड़क निर्माण में भी तेजी आई है। जहां 2013-14 में 4,260 किमी प्रति वर्ष तैयार होती थी, वहीं 2020-21 में तीन गुना बढ़कर 13,327 हो गया।
 चीन सीमा पर कुल 61 सड़कों का निर्माण
चीन सीमा पर कुल 61 सड़कों का निर्माणप्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र की सत्ता संभालते ही जहां पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की, वहीं देश की सीमाओं पर बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर दिया। सीमा पर सेना की पहुंच को आसान और तीव्र बनाने के लिए मोदी सरकार ने फंड और अन्य सुविधाएं देने में काफी तेजी दिखाई, जिसका नतीजा है कि चीन सीमा से लगी 61 रणनीतिक सड़कों की कनेक्टिविटी करीब-करीब पूरी कर ली गई है। सरकारी दस्तावेज के अनुसार, अरुणाचल, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर (लद्दाख सहित), उत्तराखंड और सिक्किम में चीन सीमा पर कुल 61 सड़कों का निर्माण चल रहा था। इनमें अरुणाचल में 27, हिमाचल में 5, कश्मीर में 12, उत्तराखंड में 14 और सिक्किम की 3 सड़कें शामिल हैं। इनकी कुल लंबाई 2323.57 किलोमीटर है।
चीन के विरोध के बाद भी गलवान नदी पर बना पुल
पूर्वी लदाख की गलवान घाटी में सेना के इंजीनियरों ने 60 मीटर लंबे उस पुल का निर्माण पूरा कर लिया, जिसे चीन रोकना चाहता था। गलवान नदी पर बने इस पुल से भारत-चीन सीमा के इस संवेदनशील सेक्टर में भारत की स्थिति बहुत मजबूत हो गई है। गलवान नदी पर बने इस पुल की मदद से अब सैनिक वाहनों के साथ नदी पार कर सकते हैं। गलवान पर पुल बनने के बाद भारत के जवान 255 किलोमीटर लंबे रणनीतिक डीबीओ रोड की सुरक्षा कर सकते हैं। यह सड़क दरबुक से दौलत बेग ओल्डी में भारत के आखिरी पोस्ट तक जाती है।
भारत-पाक सीमा पर 2100 किलोमीटर लंबी सड़कें
इसके अलावा, सरकार पाकिस्तान से लगे पंजाब और राजस्थान के इलाकों में 2100 किलोमीटर लंबे मुख्य और संपर्क मार्ग का भी निर्माण जारी है। ये सड़कें भारत के लिए रणनीतिक तौर पर काफी अहम होंगी। राजस्थान में 945 किलोमीटर मुख्य और 533 किलोमीटर संपर्क मार्ग, जबकि पंजाब में 482 किलोमीटर मुख्य और 219 किलोमीटर संपर्क मार्ग बनाए जा रहे हैं।
20 हजार गांवों में बिछेगा सड़कों का जाल
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गांवों के समग्र विकास के लिए कार्य कर रही है। मोदी सरकार का स्पष्ट मानना है कि जब गांवों का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। किसी भी क्षेत्र के विकास में सड़क, संपर्क मार्ग, यातायात के साधन अहम भूमिका निभाते हैं। इसीलिए मोदी सरकार का जोर देश के एक-एक गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने का है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत रिकॉर्ड स्तर पर सड़कें बनाई गई हैं।
 नक्सल प्रभावित इलाकों में भी सड़क निर्माण
नक्सल प्रभावित इलाकों में भी सड़क निर्माणमोदी सरकार का मानना है कि विकास के जरिए ही हिंसा और नक्सलवाद की समस्या को खत्म किया जा सकता है। इसके लिए नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क निर्माण पर सरकार का खास ध्यान है। देश में कई राज्यों में नक्सल प्रभावित ऐसे इलाकों में सड़कें बनाई जा रही हैं, जहां अभी तक किसी के जाने की हिम्मत तक नहीं होती थी। नक्सल प्रभावित इलाकों में कुल 268 सड़कों के लिए 4134 किमी लंबाई की सड़कों के बनाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसके लिए 4142 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। ये सड़कें बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ओडिसा और मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित इलाकों में बनाई जाएंगी।
भारतमाला परियोजना फेज-1 के तहत 24,800 किलोमीटर का काम पूरा
भारतमाला परियोजना के तहत देश के पश्चिम से लेकर पूर्व तक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सड़कों का जाल बिछाने की योजना है। इसके लिए नेशनल हाईवे के 53,000 किलोमीटर के हिस्से की पहचान की गई है जिसके फेज-1 में 2017-18 से 2021-22 तक 24,800 किलोमीटर के काम को पूरा किया जाएगा। इसके दायरे में नेशनल कॉरिडोर के 5,000 किलोमीटर, इकोनॉमिक कॉरिडोर के 9,000 किलोमीटर, फीडर कॉरिडोर और इंटर-कॉरिडोर के 6,000 किलोमीटर, सीमावर्ती सड़कों के 2,000 किलोमीटर, 2,000 किलोमीटर कोस्टल और पोर्ट कनेक्टिविटी रोड और 800 किलोमीटर के ग्रीन-फील्ड एक्सप्रेसवे आते हैं। फेज-1 पर लगभग 5 लाख 35 हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि फेज-1 के इस पूरे कार्य के दौरान रोजगार के करीब 35 करोड़ श्रमदिवसों का सृजन होगा।
सेतु भारतम से सड़क पर सुरक्षा
मार्च 2016 में लॉन्च की गई इस योजना का मकसद है सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसके तहत सभी नेशनल हाईवे को रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास बनाकर रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना है। 1500 पुराने और जीर्णशीर्ण पुलों को नए सिरे से मजबूती के साथ ढालना है और चौड़ा करना है। 20,800 करोड़ की लागत से 208 रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है।
चारधाम महामार्ग विकास परियोजना
27 दिसंबर 2016 को लॉन्च की गई इस परियोजना का मकसद है हिमालय में स्थित चारधाम तीर्थ केंद्रों की कनेक्टिविटी को बेहतर करना। इससे तीर्थयात्रियों का सफर और अधिक सुरक्षित, तेज और सुविधाजनक होगा। नेशनल हाईवे के करीब 900 किलोमीटर के हिस्से के आसपास होने वाले इस कार्य की अनुमानित लागत है करीब 12,000 करोड़ रुपये।